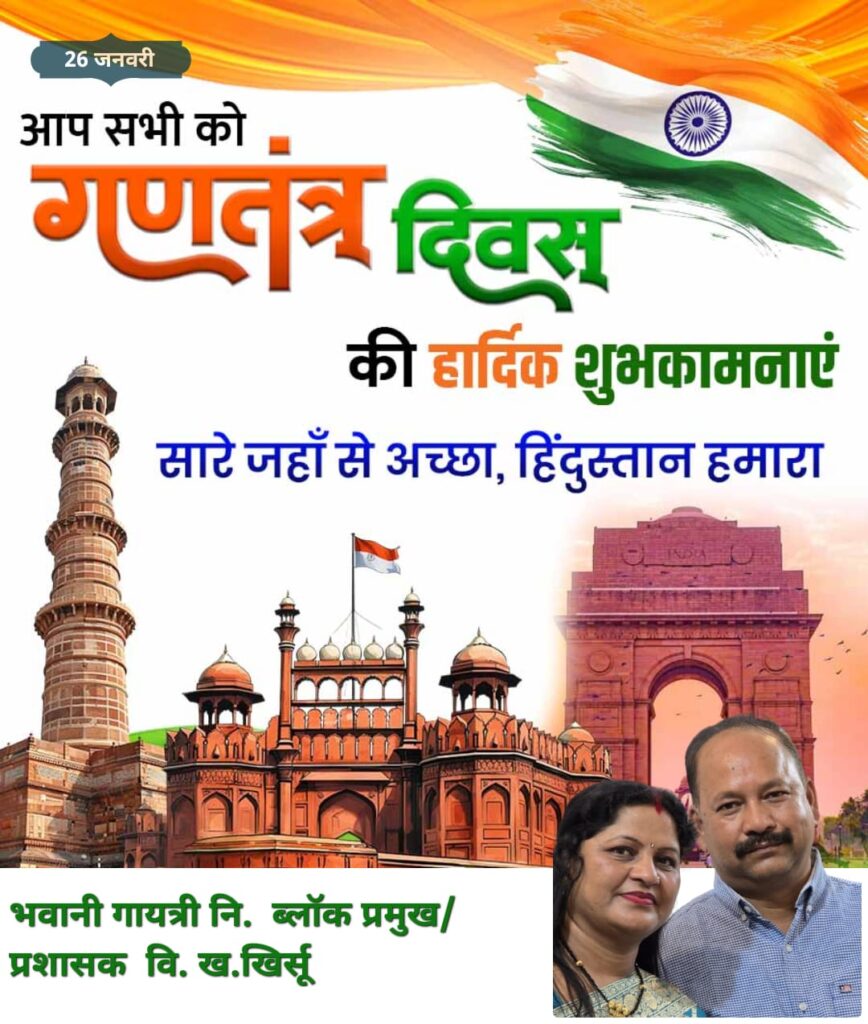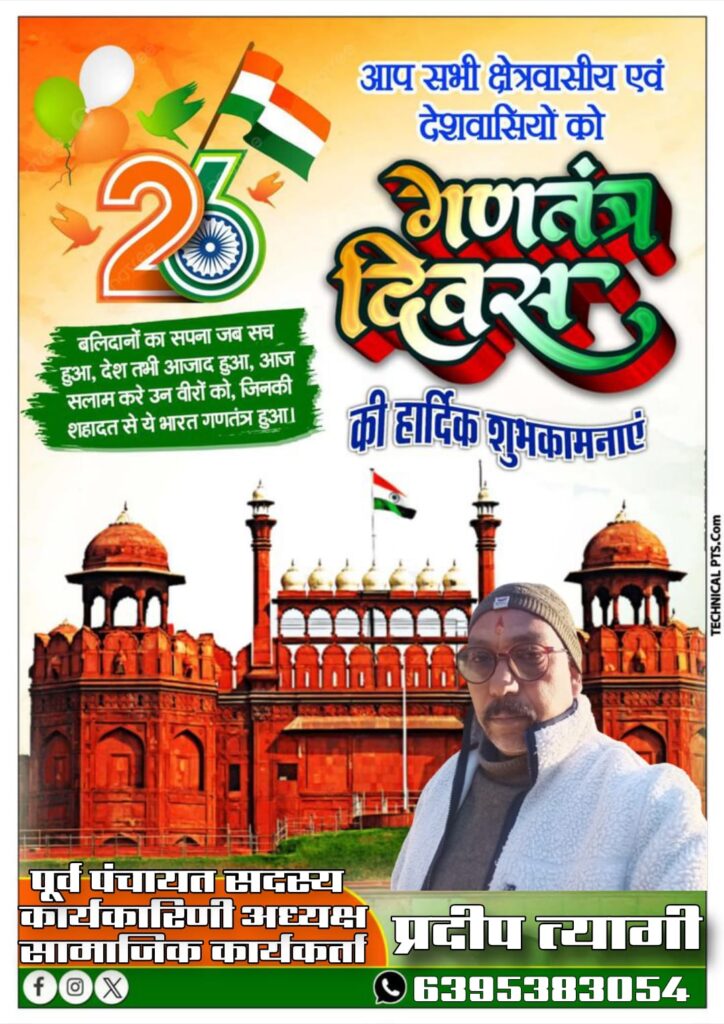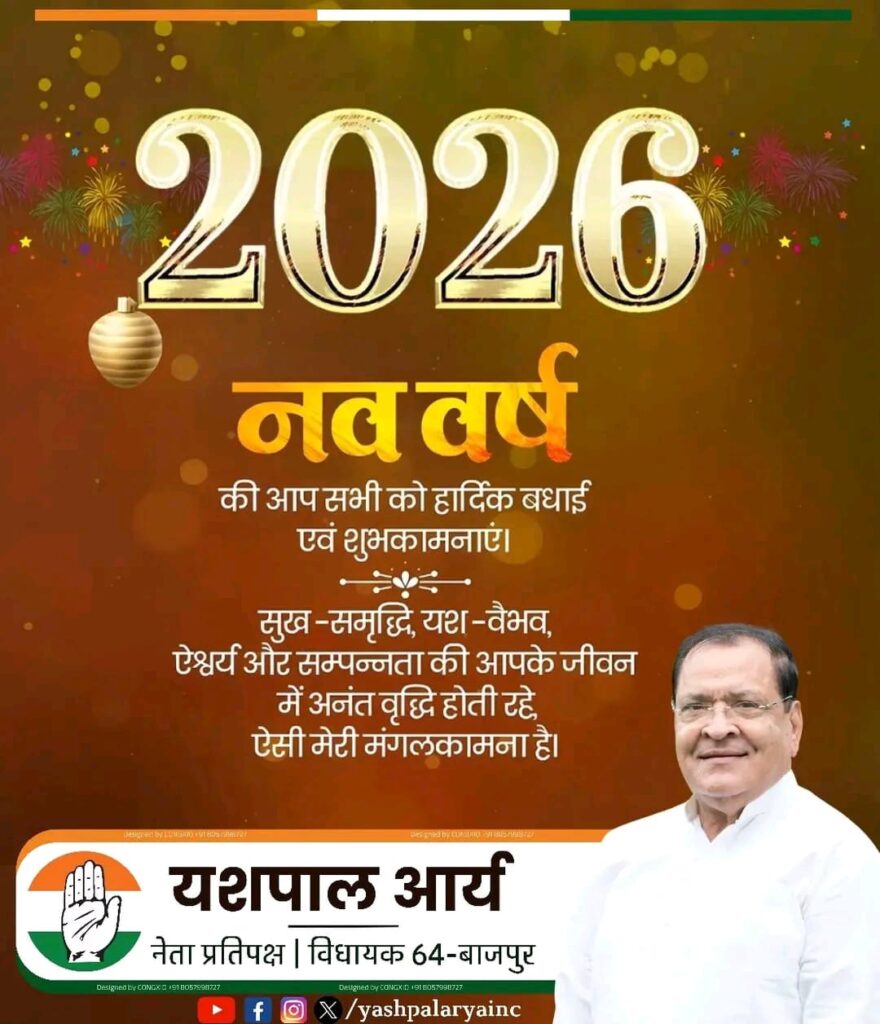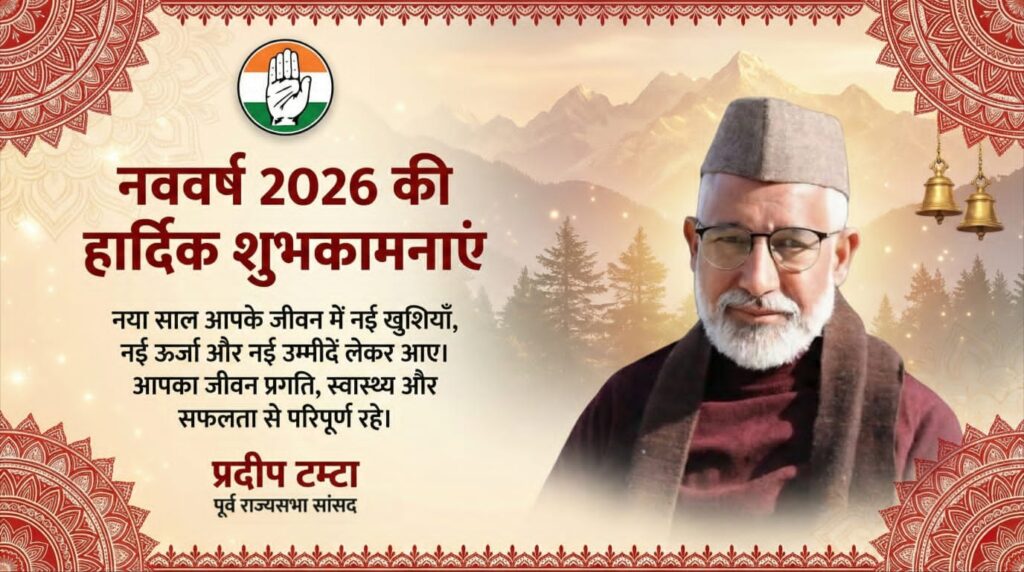उत्तराखण्ड
प्रो. लक्ष्मण सिंह बिष्ट ‘बटरोही’ धारा के विरुद्ध सशक्त प्रवाह
‘‘…ईमानदारी से जीने के लिए आदमी को जीवन – भर छटपटाना, भटकना, नये प्रयासों की शुरुवात और छोड़ना, फिर से नई शुरुवात और छोड़ना अर्थात क्षण – प्रतिक्षण गलतियां करते हुए निरंतर संघर्ष करना बखूबी आना चाहिए। इत्मीनान और चैन तो जीवन में मात्र क्षणिक मानसिक पड़ाव हैं।’’
लेव तोलस्तोय (सन् 1828 – 1910)
प्रो. लक्ष्मण सिंह बिष्ट ‘बटरोही’ की लिखित पुस्तकें ‘पहाड़ की जड़ें’ ( दख़ल प्रकाशन – 2015 ) और ‘गर्भगृह में नैनीताल’ ( मेधा बुक्स – 2013 ) पढ़ने के बाद लेव तोलस्तोय का अपने बारे में उक्त जीवन – सार मेरे आस – पास जीवंत हो गया है। इन पुस्तकों में अपने पैतृक परिवेश, इतिहास, मिथक, परम्पराओं आदि के प्रति छटपटाहट और कसमसाहट की शब्द – यात्राओं से मुझे बाहर आने में मुश्किल हो रही है।
उत्तराखंड़ी समाज के अतीत की ये शब्द – यात्रायें वैसी नहीं हैं जैसी उनके बारे में अधिकांश जगह मैनें – आपने – हमने पढ़ा – सुना है। ये तो वर्तमान पहाड़ी परिदृश्य के अंदर छुपाये परिदृश्य को बाहर की खुली ताजी हवा में लाने जैसी हैं। समाज में स्थापित – संचालित मूल्यों के अंदर का असल सच बाहर आने को होगा तो बहुसंख्यक में सामाजिक बैचेनी का भाव तो आयेगा ही। तब यह बैचेनी उनमें ही क्यों मुझ जैसे सामान्य पाठक में भी स्वाभाविक तौर पर आना लाज़िमी है।
तो मैं मान लूं इतिहास ( संदर्भ – उत्तराखंड ) में जो बोला और लिखा गया है वो सच के करीब हो सकता है, पर असल सच नहीं है। असल सच की आड़ में ही बखूबी से असल सच को हमेशा छुपाया – दबाया गया है। यही छुपाया और दबाया गया असल सच का लूला – लंगडा रूप ही हमारे आस – पास परोसा और बिखेरा गया है।
इतिहास के हर काल में बलशालियों ने बड़ी चतुराई से असल सच को अपाहिज बना कर उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने में परम्परागत महारथ हासिल की है। जन – कल्याण के सुनहरे आवरण में पहाड़ी समाज का नियामक बनने का उनका यह खेल आज भी जारी है। इतिहास में दर्ज विद्रोह जिस वर्ग के अन्याय और अनीति के विरुद्ध जीते गए समय के अतंराल ने उनके प्रतीकों – परिणामों को पुनः उसी वर्ग के हितों के अनुरूप ढ़ाल दिए हैं। हमारे समाज के ‘भीतर की असल सच्चाई’ यही है। इतिहास नायक – लोक देवता ‘कलबिष्ट’ को ही ले लो ना-
‘‘….सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि कलबिष्ट को आज उसी पुरोहिती परंपरा का हिस्सा बना दिया गया है, जिसके समानांतर एक आम पहाड़ी आदमी के मूल्यों को स्थापित करने के लिए कलबिष्ट ने सारी जिंदगी संघर्ष किया।….मंदिर में कलबिष्ट देवता जरूर बन गया है, मगर वहां वह धर्म के ठेकेदारों के हाथ की कठपुतली बना हुआ अंधविश्वासों से जकड़े निरीह पहाड़ी समाज को नचा रहा है।….कलबिष्ट की यह गाथा धर्म और सामंती शोषण से ग्रस्त उस उत्पादक वर्ग की पीड़ा का भी आख्यान है जहां शोषक उत्पादक को हाशिए में धकेल कर उसे इस कदर अकेला छोड़ देता है कि वह एक सीमा के बाद अपने ही शोषक को पूजने लगता है।’’
( ‘पहाड़ की जडें’ पृष्ठ 110 – 112 )
बटरोही की ख्याति देश – दुनिया और हिन्दी साहित्य में एक कहानीकार के रूप में है। उनकी कहानियां स्मृतिपटल पर खिंचे वे रेखाचित्र हैं जो अपने परिवेश से बाहर नहीं जाते हैं। अपने समाज के दुखः – सुख में रचे – बसे पात्रों के मन – मस्तिष्क के द्वन्द्वों को उन्होने कहानी का रूप दिया है। यही कारण है कि उनके पात्र बोलते कम और सोचते बहुत ज्यादा हैं-
‘सोचती है लछिमा। उसकी हालत भी ठीक घुघते जैसी है। जब चारों ओर से हिंसक आंखे उसे घेरे रहती है तो कोई ऐसा रास्ता भी नहीं बच पाता जहां से वह भाग सके। भीड़ के बीचों – बीच से उड़कर आकाश में नहीं जा सकती वह। घुघुते के पास तो पंख हैं, उसके पास तो वे भी नहीं हैं। आंखे बंद कर लेने के सिवा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्या करे वह? सोचती है लछिमा। लेकिन कह नहीं पाती। एक तो कह नहीं पाती, दूसरे सोचती है कि ऐसी बातें कहे भी तो किससे? कौन सुनेगा उसके मन की ऐसी बातें?’
( ‘लछिमा’ कहानी का विराम अंश )
‘बटरोही’ की इस कहानी में पहाड़ की स्त्रियों का मौन बयान है। परन्तु मुझे इससे ज्यादा यह लगता है कि बटरोही जी अपनी मूक वेदना की अभिव्यक्ति के लिए ‘लछिमा’ को सामने लाये हैं। समाज में परम्पराओं की जड़ें अभिमान और अपमान का पैगाम एक साथ लिए रहती – आती हैं। यही सामाजिक अभिमान और अपमान का द्वन्द्व बटरोही के लेखन का केन्द्र है।
बटरोही जी का संघर्ष बाहर से नहीं अपने आप से है। सामाजिक परम्पराओं के प्रचलित पूर्वाग्रह – दुराग्रह आदमी को कितना बेबस – बैचेन करते हैं यह उनके लेखकीय संघर्ष में बखूबी दिखता है।
‘‘….जिन शब्दों और संदर्भों को मैं स्वयं के लिए आपत्तिजनक समझता था, उन्हें तो सम्मान की नजर से देखा जाने लगा है और जो हमारे आदर – सूचक शब्द थे, वे व्यंग्य और निरादर की छवि देने लगे हैं ( पृष्ठ 9 )।’’ ‘‘ठहरे तो खशिए ही! खून का असर थोड़े ही जाता है कभी….( पृष्ठ – 56 )।’’ ‘‘सत्यानाश!….इतना पढ़ – लिख कर भी तुम हमारे गोत्र और प्रवर नहीं जानते हो भाई! तुमको क्या हमें बताना पडे़गा कि हम लोग कुलीन क्षत्रिय हैं ( पृष्ठ- 75 )।’’
( ‘पहाड़ की जडें’ )
‘‘….अपनी चौड़ी हथेली से उन्होने मुझे एक झन्नाटेदार चांटा जड़ा और जीवन की पहली दीक्षा दी कि तुम गंवार लोग कभी सुधर नहीं सकते….बिशनगुरू के अनुसार, ऐसे बज्र – दिमाग खसियों कोे पढ़ने की नसीहत पता नहीं कौन देता है? अगर ये न भी पढ़ते तो धरती पर कौन – सा प्रलय आ जाता?’’
( ‘गर्भगृह में नैनीताल’, पृष्ठ – 24 )
सामाजिक सुरक्षा कवचों से घिरे लोग अंदर से कितने डरे होते हैं, ये वे बार – बार बताते हैं। अपनी सामाजिक सत्ता के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उनके कारनामों की पोल बटरोही बार – बार खोलते हैं। निःसंदेह पुरातन सामाजिक परंपराओं को छीलना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है-
‘‘….आदमी का क्या भरोसा है साब….उसे समझना इतना ही आसान होता तो आज नौलखिया के गांव वालों को हम इस तरह उनके ग्वाले को पूजते हुए नहीं देखते! आप इतनी दूर से एक खशिए को पूजने के लिए नहीं आते और मैं यहां इस कुर्सी पर नहीं बैठा होता। हमारे पुरखों को तो कोई भी मंदिर के अंदर घुसने नहीं देता था, चाहे वो कलबिष्ट हो या सम्राट पांडेज्यू! इनको सब माफ है साहब….भिना – साले की लड़ाई से हमको क्या मतलब हो रहा है….हम क्यों पड़ें उनके बीच में! कर खांए जैसे चाहते हैं।….हमें तो अपना हिस्सा घर बैठे ही मिल जाता है भैय्या!’’
( ‘पहाड़ की जडें’, पृष्ठ 178 – 179 )
‘बात यह है दोस्त, जब व्यवस्था के द्वारा भेजी गई राख उनके शरीर पर पड़ती है तो वे लोग एक नए आदमी को जन्म देते हैं….जो उन्हीं की तरह सोचता है, और बिना बताए ही उसे मालूम हो जाता है कि खाक के बोरों का क्या करना है। वह बोरों को देखते ही चिल्लाता हुआ उन्हें अपने सिर पर रख लेता है और व्यवस्था के गुणगान करने लगता है।’ ’
( ‘किम्पुरुष’, ‘पहाड़ की जडें’, पृष्ठ – 43 )
बटरोही की इन दोनों किताबों में लेखन के एक नये प्रयोग और राह की संभावनाओं ने अपनी जगह बनाई है। ये महज आत्मकथा और आत्मसंस्मरण तो कदापि नहीं हैं। क्योंकि ज्यादातर आत्मकथाओं और संस्मरणों में दिखाई देने वाली आत्ममुग्घता यहां सिरे से गायब है। अपनी जीवनीय वापसी की इस यात्रा में बटरोही जी द्वारा अपने और सामाजिक परिवेश के प्रति अपनाई तटस्थता – निष्ठुरता उनको सच लिखने को प्रेरित करती है और अतीत को महामंडित करने से रोकती है।
ये किताबें आज के जाति – क्षेत्र के अभिमान और अहम से चिपटे समाज से ज्यादा आने वाली चेतनशील पाठक पीढ़ी के मन – मस्तिष्क के करीब हैं। अतः इन किताबों को हमसे ज्यादा नवजवान पीढ़ी को पढ़ना और समझना चाहिए। उन्हीं से इनकी प्रासंगिकता और उपयोगिता साबित होंगी।
ये किताबें मानती हैं कि इतिहास की परतें खोलने से उसके प्रचलित स्वरूपों – मान्यताओं में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इतिहास को निर्ममता से छीलना होगा तभी उसके भीतर बलशालियों द्वारा दुबकाये सामाजिक सच की रिहाई संभव है।
….‘‘ पापा, आपने मुझे बताया नहीं कि हम ठाकुर भंडारी हैं या ब्राहृमण भंडारी? क्या ठाकुर और ब्राहृमण भंडारी अलग – अलग होते हैं? ये जातियां बनती कैसे हैं पापा? जो लोग जानवरों का चारा खा जाते हैं, वे किस जाति के हुए और जो लोग करोड़ों रुपया छिपाकर विदेश चले जाते हैं, वो किस जाति के हुए? क्या प्रजातंत्र में ऐसी ही जातियां होती हैं पापा?….पापा, आपने बताया था कि इस देश में कभी तैंतीस करोड़ देवता होते थे और तब इतनी ही जनसंख्या भी थी। इस प्रकार उस समय हर आदमी देवता था। क्या इसी तरह आज हर आदमी नेता जी बन गया है? लेकिन मैं तो नेता नहीं हूं। आप भी तो नेता नहीं हैं।’’
( ‘पहाड़ की जडें’, पृष्ठ – 188 )
‘नैनीताल के कुलदीप’ के ये प्रश्न ज्यों के त्यों हैं। है कोई जवाब इन प्रश्नों के हमारे पास? हमें मालूम है कि इन प्रश्नों का जवाब आज की सयानी – प्रभुत्व – सम्पन्न पीढ़ी नहीं दे पायेगी अथवा नहीं देना चाहेगी। इन दोनों किताबों पर हुई चर्चायें जितनी मेरी नजर में आई हैं वे बटरोही जी के लेखन पर सिमटी – केन्द्रित हैं न कि किताबों में उठाये – उभरे प्रश्नों, शंकाओं और संभावनाओं पर। परन्तु यह उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी अपने समाज को इन प्रश्नों से निज़ात दिलायेगी। बटरोही जी का साहित्य उस भावी पीढ़ी के पास तब संदर्भ साहित्य के रूप में मार्गदर्शन करेगा।
इतिहास में दुबकाये सच की रिहाई इसलिए भी जरूरी है कि अतीत के भ्रम और भय में जीता पहाड़ी समाज आधुनिक विज्ञान – सम्मत सामाजिक चेतना को मन – मस्तिष्क से मानते हुए भी उसे अपने व्यवहार – आचरण में नहीं ला पा रहा है। अतीत से दबा, वर्तमान से भ्रमित और भविष्य से भयभीत वर्तमान पहाड़ी युवा इसीलिए अपनी पैतृक प्राकृतिक – सामाजिक विरासत को संकोचवश आत्मसात नहीं कर पा रहा है।
‘‘कहते हैं, नैनीताल की ‘खोज’ करने वाला पीटर बैरन 1841 में नैनीताल के थोकदार नर सिंह बोरा को तालाब के बीचों – बीच ले गया और उसे झील में डुबाने की धमकी देकर उस रुक्के पर अंगूठा लगवा लाया जिसके अनुसार नैनी झील और उसमें रहने वाली नैनीताल वासियों की कुलदेवी नंदा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वामित्व हो जाएगा। 2 दिसंबर, 1815 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई सिगौली – संधि के बाद क्या इस दस्तावेज की कोई जरूरत रही होगी?’’
( ‘गर्भगृह में नैनीताल’, पृष्ठ – 5 )
क्या जरूरी है कि इतिहास में जो दर्ज है उसे वैसे ही मान लिया जाय। इन किताबों में जो इतिहास में लिखा और बताया गया है, उससे इतर की कई संभावनाओं और विकल्पों को उजागर करके बटरोही नये प्रश्न उभारते हैं, तो यह तिलमिलाहट क्यों? परन्तु यह तिलमिलाहट स्वाभाविक भी है, क्योंकि अतीत पर प्रश्न उठाने का सीधा अर्थ, वर्तमान सामाजिक सत्ता की संप्रभुता को चुनौती देकर उसे असहज करना ही है।
‘पीटर ने लिखा है कि उस तालाब ( नैनीताल ) का पानी हीरे की तरह इतना साफ और पारदर्शी था कि नब्बे फीट गहरे तालाब की सतह पर बिछे पत्थरों और वनस्पतियों के रंग और आकार को ऊपर पहाड़ी के शिखर पर से साफ पहचानाा जा सकता था।’
( ‘गर्भगृह में नैनीताल’, पृष्ठ – 64 )
आज नैनीताल की झील में कितनी गंदगी समाई होगी, यह हम सब जागरूक सभ्रांत नागरिक जानते हुए भी अनदेखी करने की स्थिति में हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे समाज में वर्ग – जाति – क्षेत्र का जो अहम् और भ्रम हमारे मन – मस्तिष्क में आज भी विराजमान है, उसके सामाजिक कुप्रभावों को जानते हुए भी हम उसे छोडने को तैयार नहीं हैं।
अपने गांव चामी में रहते हुए मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर हमारा ग्रामीण समाज जातिविहीन होता तो आज हम खेती – बाड़ी ही नहीं गांव सभी संसाधनों और लोगों का हजारों गुना बेहतर उपयोग कर रहे होते। गांव के हर काम की शुरुआत में ही जाति सबसे पहले हाजिर होकर हमारे सोचने, बोलने और उसको करने की सीमाओं से हमें बांध देती है।
पहाड़ी समाज के बीते कल मैं हुए अनेकों ऐसे कई प्रसंगों से पाठकों को ये किताबें गुजारती हैं। सामाजिक दायित्वशीलता की इसी तरह की कई अन्य यादों को दिलाती ये किताबें अन्य लेखकों को भी अपने बीते जीवनीय सच की व्यापक पड़ताल करने का संदेश दे रही हैं।
‘‘….दस साल की उम्र मेें, मैं धसपड़ से नैनीताल भाग आया था हालांकि आते वक्त कई दिनों तक खड़कुवा के साथ मेरी लंबी गंभीर बैठकें हुई थीं….अपने गांव की समस्याओं और उन्हें ठीक करने के उपायों के बारे में हमने अनेक योजनायें बनाई थीं और खड़कुवा से मैंने वायदा किया था कि शहर जाकर मैं उन्हें जरूर पूरा कर लूंगा। उसने गांव से तीन मील दूर, स्कूल के पास वाली किताबों की दुकान से बादामी रंग के कवर वाली एक काॅपी चुराकर चुपके से मुझे दी थी और कहा था कि गांव को ठीक करने वाले अपने सारे सुझावों को मैं उसमें लिख लूं जिससे कि उन्हें भूलने का कोई अन्देशा न रहे। सात – आठ साल की उस कच्ची उम्र में उसने सुझाया था कि जब मैं गांव लौट आऊंगा तो हम दोनों लोग पश्चिमी पहाड़ी की चोटी वाले सबसे ऊंचे देवदार के पेड़ के नीचे बैठकर उन सारे सुझावों पर पूरे दिन बातें करेंगे और जिस वक्त थका – हारा लाल सूरज पश्चिमी पहाड़ी के क्षितिज पर हमारी पीठ को छूकर धरती के गर्भ में समा रहा होगा, हम लोग नीचे गांव की ओर उतर आएंगे।’’
( गर्भगृह में नैनीताल, पृष्ठ – 20 )
अपने बचपन के खड़कुवा जैसे मित्र से ऐसी ही सलाह – वायदा अनेकों स्थापित – लोकप्रिय व्यक्तित्वों ने भी किया होगा। आज का वक्त उसे निभाने उसके पास जाने का है। जीवन की वापसी यात्रा में हम – सबको यही अवलोकन और मूल्यांकन करना है। ये मात्र नाॅस्टेल्जिया नहीं है।
बटरोही का साहित्य सीधा – सपाट नहीं वरन जीवनीय ऊबड़ – खाबड़ में व्यक्ति के आन्तरिक द्वन्द्वों को उद्घाटित करता हुआ है। वह बताता है कि परम्पराओं की सत्ता की डोर समाज को कैसे नियंत्रित करती है। मानवीय जीवन में सामाजिक जड़ता की जड़ों को कौन, क्यों और कैसे पनाह देता रहा है।
क्या हमारा पहाड़ी समाज उतना ही सरल और सहृदय है, जितना दिखता – दिखाया या प्रचारित किया जाता है। जातीय सौहार्द्र और मधुर संबंधों का सच कुछ और ही तो नहीं है? वर्ग – जातियों की बाहृय निकटता का मूल कारण भौगोलिक विकटता और सीमित संसाधन तो नहीं है? इस तरह पहाड़ में तथाकथित परम्पराओं की जो जड़ें धसांई गई हैं, यह किताबें उसकी गहराई में जाकर चोट करती है। जीवनीय आदर्शां से ज्यादा जीवनीय आकर्षणों को पाने की लालसा इनमें समायी है।
सीधे शब्दों में बटरोही का साहित्य सहलाता नहीं है वरन सजग करता है। वह कबलाहट से आगे बड़ता है। उसकी कबलाहट पाठक को हमेशा बैचेन करती है।
‘‘हमारा उनके साथ क्या रिश्ता था? यह सवाल मेरे दिमाग में उस दिन एक तकलीफदेह जिज्ञासा के साथ उठा था, जब मैं और फरहत….उनकी चिता में आग देने के लिए जलती लकड़ियों की मशाल हाथ में लिए चिता के चक्कर लगा रहे थे।….चिता को या तो बेटा अग्नि देता है या कोई निकटतम संबंधी। फरहत तो धर्म, जाति या रिश्ते से न मेरा संबंधी था, न उनका। मैं धर्म से जरूर उनसे जुड़ा था, मगर उनके साथ मेरा कोई रिश्ता दूर – दूर तक नहीं था। फरहत तो मुसलमान था, जिसके धर्म में किसी मृत व्यक्ति को इस प्रकार चिता में आग नहीं दी जाती थी। तब हम लोग यह नाटक क्यों कर रहे थे?….क्या ये सब करने का हमें ये अधिकार था? अगर अधिकार ही नहीं था तो यह कर्मकांड रचने की क्या जरूरत थी? मगर यह सारी प्रक्रिया भले ही नाटक – जैसी लग रही हो, उस वक्त तो वह एक जीती – जागती वास्तविकता थी।’’
( ‘गर्भगृह में नैनीताल’, पृष्ठ – 177 )
छाना गांव, अल्मोड़ा में 25 अप्रैल, 1946 को जन्में प्रो. लक्ष्मण सिंह बिष्ट ‘बटरोही’ विगत 55 वर्षों से लेखन में सक्रिय रहते हुए वर्ष – 2006 में कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल से विभागाध्यक्ष ( हिंदी ) और अधिष्ठाता कला संकाय के पद से सेवा – निवृत्त हुए। वे वर्ष – 1997 से 2000 तक ‘ऑत्वाॅश लोरांद विश्वविद्यालय, बुदापैश्त’ ( हंगरी ) में हिंदी के विजिटिंग प्रोफ़ेसर रहे।
बटरोही जी के 5 कहानी संग्रह ( दिवास्वप्न, सड़क का भूगोल, अनाथ मुहल्ले के ठुल – दा, हिडिम्बा के गांव में ), 5 उपन्यास ( बर्फ, महर ठाुकुरों का गांव, थोकदार किसी की नहीं सुनता, आगे के पीछे ), शोध – आलोचना – संपादन ( गांधी संदर्भ, इक्कीसवीं सदी में गांधी, About Gandhi, कुमाउंनी संस्कृति, हिंदी कहानी के अट्ठारह कदम ), बाल साहित्य ( एक ही धारा, सुबह का भूला, सुदामा, वीर गाथाएं ) आदि प्रकाशित साहित्य हैं।
नैनीताल के निकट रामगढ़ में महादेवी वर्मा के घर ‘मीरा कुटीर’ की ‘महादेवी वर्मा सृजन पीठ’ के वे संस्थापक रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के अनेक सम्मानों से नवाज़े बटरोही जी की लेखकीय यात्रा जारी है।
वास्तव में ‘पहाड़ की जडें’ और ‘गर्भगृह में नैनीताल’ किताबें विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक, मानवीय परिस्थितियों एवं परिवेश में जी रहे लोगों के ‘भीतर की सच्चाई’ है। उनके निजी सुख – दुःख, खुशियां, उल्लास, इच्छाओं, आचार, व्यवहार और सोच का अदभुत संयोजन है, ये किताबें।
इन किताबों में कलबिष्ट, गंगनाथ, गौलू, मैद सोन, चौमू, पैकों (मल्ल) की दुनिया, हल्दुवा – पिंगलुवा, राजुला मालूशाही, ग्वाल्देकोट की गोपुल्दी, शेरुवा पैक, गजू लाट, नैनीताल का कुलदीप, लक्षुवा कोठारी, इनरुवा जोगी, दाड़िमी माई, बंपुलिस, रूसी गांव की खष्टी बुआ, बाबजी, पुष्पा दीदी, रोज़ी एडवर्ड, ठुल-दा, गरुड़ध्वज जोशी, चिलम सौज्यू, लाल खबीस, मिसेज रेनू बनर्जी, बड़बाज्यू, फरहत, खड़कुवा, बिशनगुरू, खुशाली बुआ, जसवंता, परमेश्वरी, करीम दर्जी, शंकरिया केवट, सुमित्रानंदन पंत, शैलेश मटियानी, बद्री दत्त पांडे, महेंद्र सिंह धौनी, हरीश रावत, विजय बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, अभिताभ बच्चन, रजनी रावत, पीटर बैरन, थोकदार नर सिंह बोरा, विलियम ट्रेल, जिम काॅर्बेट और भी कई अन्य व्यक्तित्व अपने बेहतरीन किरदारों में हैं।
उक्त सब किरदारों का ‘बीटिंग द रिट्रीट’ – ‘विजय के बाद वापसी का मार्चपास्ट’ वाला खुली आंखों का सपना प्रो. बटरोही जी ने देखा और उसे हू – ब- हू आप तक इन किताबों के माध्यम से पहुंचाया है। और आप जानते ही हैं कि खुली आंखों से देखे गए सपने बहुत प्रभावी और असरदार होते हैं जो दूर – भावी मंजिल का अहसास भी कराते हैं। इसीलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये किताबें नवजवान पीढ़ी को पहाड़ी समाज को समझने के लिए संदर्भ ग्रंथ साबित होंगी।
आदरणीय देवेन्द्र मेवाड़ी जी, प्रिय शिरीष कुमार मौर्य जी और प्रदीप पांडे जी ने अपनी – अपनी विधाओं से इन किताबों को आकर्षक कलेवर प्रदान कर इन पुस्तकों के तथ्य – कथ्य – मर्म को मनभावन सजीवता प्रदान की है।
डाॅ. अरुण कुकसाल